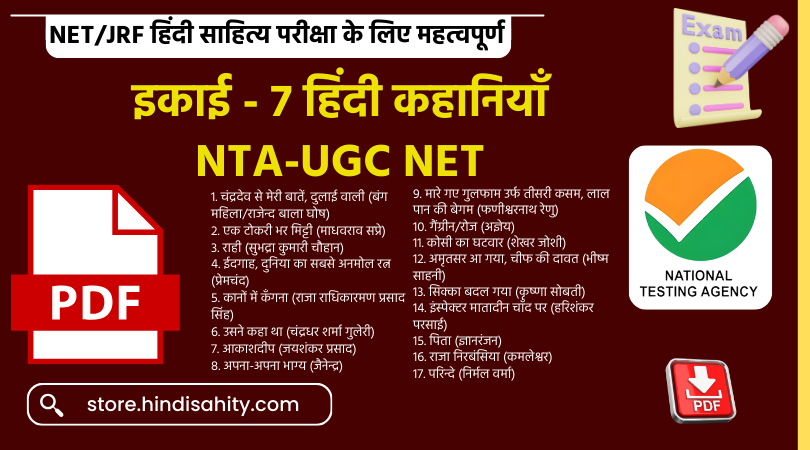एकांकी के तत्व कितने होते हैं
एकांकी के तत्व(Ekanki Ke Tatva Bataiye): आज के आर्टिकल में हम गद्य विधा में एकांकी के तत्त्व पर जानकारी शेयर करेंगे।
एकांकी के तत्व – Ekanki Ke Tatva
एकांकी के प्रमुख तत्त्व कथावस्तु,पात्र एवं चरित्र चित्रण,संवाद,देशकाल एवं वातावरण,अभिनेयता और उद्देश्य होते है एकांकी के मुख्यत: छ: तत्त्व होते है।
एकांकी की परिभाषा:
एक अंक वाला नाटक एकांकी नाटक या एकांकी कहलाता है। कहानी की भाँति एकांकी नाटक भी एक घटना, एक परिस्थिति और एक उद्देश्य से बनता है-हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाटक और एकांकी में वही संबंध और अंतर है जो उपन्यास और कहानी में होता है। प्रभावोत्पादन की दृष्टि से एकांकी भी उतनी ही सफल नाट्य विद्या है जितना कि नाटक।
डॉ. रांगेय राघव प्रभृति विद्वान् एकांकी को पाश्चात्य One Act Play का हिंदी रूपान्तरण मानते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी (मंदिर, बादलों के पार), विष्णु प्रभाकर (अशोक, इंसान, क्या वह दोषी थी, 12 एकांकी, प्रकाश और परछाई), लक्ष्मीनारायण मिश्र (मुक्ति का रहस्य, राजयोग), मोहन राकेश (अंडे के छिलके), भुवनेश्वर (कारवाँ, आदमखोर, इंस्पेक्टर जनरल), उदयशंकर भट्ट (आज का आदमी, जवानी और 6 एकांकी) हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं।
एकांकी के निम्नांकित छ: तत्त्व माने गये हैं –
- कथावस्तु
- पात्र एवं चरित्र चित्रण
- संवाद
- देशकाल एवं वातावरण
- अभिनेयता
- उद्देश्य
📄📑📕📝 हिंदी साहित्य से जुड़ी सभी भर्तियों के लिए टॉप नोट्स 📝📝📝💯💯📂
| हिंदी साहित्य का आदिकाल(विवरणात्मक), 67 पेज | Click Here |
| हिंदी साहित्य का भक्तिकाल(विवरणात्मक), 60 पेज | Click Here |
| हिंदी साहित्य का रीतिकाल(विवरणात्मक), 32 पेज | Click Here |
| हिंदी साहित्य का आधुनिक काल(विवरणात्मक), 75 पेज | Click Here |
| हिंदी साहित्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न(5000 Q) | Click Here |
| हिंदी साहित्य का आदिकाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न(1000 Q) | Click Here |
| हिंदी साहित्य का भक्तिकाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न(1000 Q) | Click Here |
| हिंदी साहित्य का रीतिकाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न(1000 Q) | Click Here |
| हिंदी साहित्य का आधुनिक काल ऑब्जेक्टिव प्रश्न(2000 Q) | Click Here |
| UGC NET हिंदी साहित्य(सम्पूर्ण 10 इकाई) | Click Here |
1. कथावस्तु –
कथावस्तु एकांकी का अनिवार्य एवं मूल तत्व है, जिसके बिना एकांकी की कल्पना नहीं की जा सकती। एकांकी की कथावस्तु किसी एक घटना, प्रसंग, एक चरित्र, एक कार्य इत्यादि पर आधारित होती है। इसमें आधिकारिक अर्थात् मूल कथा ही होती है, प्रासंगिक कथाओं (गौण कथाओं) का इसमें स्थान नहीं होता है। एकांकी की कथा प्रारंभ होते ही सीधे लक्ष्य (चरम) की ओर अग्रसर होती है। आरम्भ, चरम एवं अंत ही एकांकी की कथावस्तु की अवस्थाएँ हैं। संक्षिप्तता, सांकेतिकता, मार्मिकता, कौतूहलता, मौलिकता, रोचकता एवं प्रभावान्विति एकांकी के अच्छे कथानक के मुख्य गुण हैं।
2. पात्र एवं चरित्र चित्रण –
पात्र एवं चरित्र-चित्रण एकांकी का दूसरा प्रमुख एवं अनिवार्य तत्त्व हैं। एकांकी का फलक सीमित होता. है इसलिए इसमें कम-से-कम गिने-चुने पात्रों की योजना की जाती है। तथा पात्रों का चरित्र – चत्रिण भी रेखाचित्रात्मक स्वरूप में ही संभव हो पाता है। पात्रों का चरित्र-चित्रण एकांकी में जीवंत, विश्वसनीय, गतिशील एवं प्रभावशाली रूप में होना चाहिए ताकि प्रेक्षक उसे आसानी से पचा सके।
डॉ. रामकुमार वर्मा का मत है कि- “घटना से अधिक शक्तिशाली पात्र होते हैं। एकांकी में पात्र महारथी होता है। घटनाएँ रथ बनकर समस्या-संग्राम में उसे गति प्रदान करती हैं।” आज एकांकी में संघर्ष (मानव-जीवन की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न घात-प्रतिघात) को भी अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है और इसे भी एकांकी का एक अन्य तत्त्व माना जाने लगा है।
3. संवाद –
संवाद, कथोपकथन अथवा डायलॉग एकांकी का प्राणतत्त्व है। कथावस्तु एवं पात्रों के चरित्र-चित्रण की सफलता संवादों पर ही आधारित होते हैं। एकांकी के संवाद कथा-विकास एवं चरित्र-चित्रण के विकास में समर्थ होने चाहिए। संक्षिप्तता, रोचकता, ध्वन्यात्मकता, सजीवता, स्वाभाविकता इत्यादि विशेषताएँ भी एकांकी के संवादों में अपेक्षित हैं। संवादों की भाषा-शैली सरल, सहज, बोधगम्य एवं प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।
4. देशकाल एवं वातावरण –
‘देश’ का तात्पर्य है- ‘स्थान’; ‘काल’ का अर्थ है- ‘समय’ एवं ‘वातावरण’ से अभिप्राय है— ‘परिवेश’। चूँकि एकांकी का ‘कैनवस’ लघु होता है, इसलिए इसमें देशकाल एवं वातावरण के विस्तृत विश्लेषण की गुंजायश नहीं होती, सिर्फ एकांकी में इसका आभास मात्र होता है।
5. संकलन-त्रय –
एकांकी में संकलन-त्रय (स्थान, समय एवं कार्यघटना की एकता) का निर्वाह एकांकी में सौंदर्य की सृष्टि हेतु आवश्यक है। डॉ. रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर सरीखे प्रसिद्ध एकांकीकार एकांकी में संकलन-त्रय का निर्वाह आवश्यक मानते हैं जबकि डॉ. नगेन्द्र सरीखे आलोचकों की यह मान्यता है कि एकांकी में संकलन-त्रय के प्रति अधिक आग्रह नहीं होना चाहिए।
6. अभिनेयता –
अभिनेयता एकांकी का वह केन्द्रीय तत्त्व है जिसकी मंच पर अभिनीत होने में है। चूंकि एकांकी दृश्यकाव्य है, इसलिए एकांकी अभिनेय होता है। एकांकी में अभिनय के चारों प्रकारों – आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्त्विक का प्रयोग होता है।
7. उद्देश्य –
‘उद्देश्य’ एकांकी का अंतिम वह तत्त्व है, जिसकी प्रेरणा से वशीभूत होकर कोई एकांकीकार ‘एकांकी’ का सृजन करता है। रसास्वादन, आनंदोपलब्धि, किसी समस्या का समाधान, मानव जीवन की एक स्थिति विशेष का चित्रण इत्यादि कुछ भी एकांकी का उद्देश्य हो सकता है। यह उद्देश्य एकांकी में आरोपित न होकर अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होना चाहिए।
इस प्रकार, एकांकी के इन तत्त्वों के समावेश से ही एकांकी की दृश्य – काव्यता सिद्ध होती है।
Search Queries:
ekanki ke tatva bataiye,ekanki ke tatva ke naam likhiye,एकांकी के तत्व बताइए,ekanki ke tatva,एकांकी के तत्व,ekanki ke kitne tatva hote hain,एकांकी के कितने तत्व होते हैं नाम लिखिए,ekanki ke tatva par prakash daliye,एकांकी के तत्व कितने होते हैं