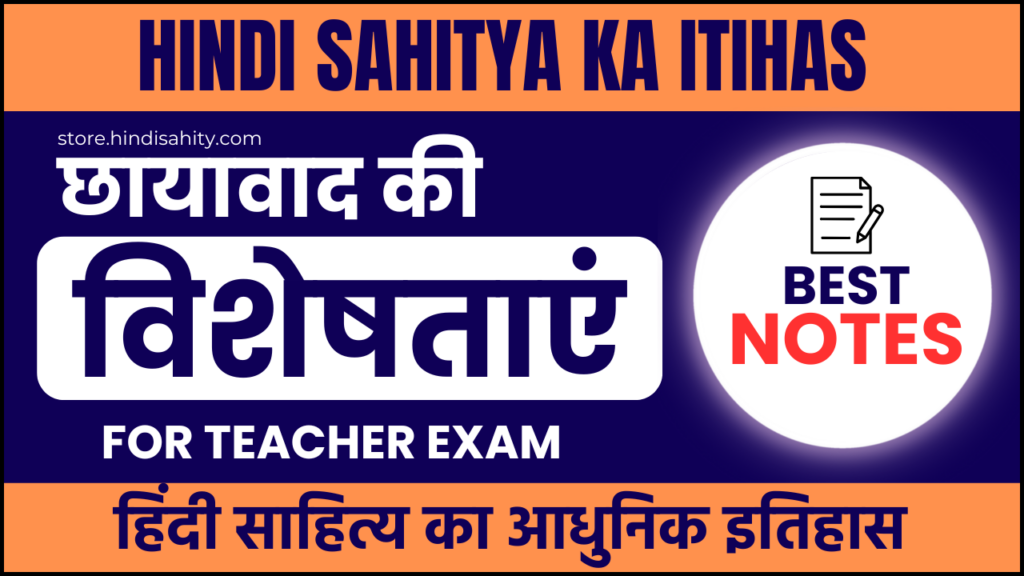द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएँ
द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएँ (Dwivedi Yugin Kavya ki Visheshtaen): आज के आर्टिकल में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अन्तर्गत द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं पर सम्पूर्ण जानकारी शेयर करेंगे।
द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएँ
हिंदी-साहित्येतिहास में 1900 से 1918-20 ई. तक का काल द्विवेदी काल है। समकालीन साहित्य पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली व्यक्तित्व की इतनी गहन व प्रभावशाली छाप पड़ी कि उनका युग (1900-1918) ‘द्विवेदी युग’ कहलाया। जागरण और सुधार की दृष्टि से यह काल ‘जागरण सुधार काल’ भी कहा जाता है। द्विवेदी जी के अतिरिक्त मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ इत्यादि द्विवेदीयुग के प्रधान कवि थे।
1. राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता द्विवेदीयुगीन कव्य की प्रधान भावधारा थी। द्विवेदीयुगीन कवियों ने देश की वर्तमान हीन दशा पर क्षोभ प्रकट किया और आलस, फूट, मिथ्या, कुलीनता इत्यादि को उसका कारण बताया। उन्होंने परतंत्रता को सबसे बड़ा अभिशाप मानते हुए स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी।
‘’देशभक्त वीरों मरने से नहीं नेक डरना होगा।
प्राणों का बलिदान देश की बलिवेदी पर करना होगा।।‘’
2. जागृति
द्विवेदीकाल ‘जागरण काल’ है। यह राष्ट्रीय जागृति का वह काल है, जब सारा देश अंगड़ाई लेता हुआ जागता है। ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जेहाद के रूप में उभरता हुआ आक्रोश द्विवेदी युग में देखते ही बनता है। वस्तुतः भाषा, विषय, राष्ट्रीयता इत्यादि विभिन्न आधारों पर द्विवेदी युग समस्त देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काल है।
3. काव्यफलक का विस्तार
‘सब विषय काव्योपयुक्त हैं, कविता के क्षेत्र में द्विवेदीयुग में यह मार्ग प्रशस्त हुआ। चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक, बिंदु से लेकर समुद्र तक, अनंत आकाश, अनंतपृथ्वी, अनंतपर्वत इत्यादि सभी को काव्य का उपयुक्त विषय माना गया।
4. मानवतावाद
द्विवेदीयुग में सामान्य मानव की प्रतिष्ठा पहली बार हुई। छायावाद-युग में जो सामान्य मानव आता है, वह द्विवेदीयुग से ही चलकर आता है। द्विवेदी जी की कविता में ‘कल्लू अल्हैत’ काव्य का विषय बना, तो अविद्यानंद के व्याख्यान में विदेशीयता का रसिक शंकर जी के व्यंग्य बाण का लक्ष्य बना। द्विवेदी युग में साकेत, द्वापर, यशोधरा में उपेक्षित नारियों का चित्रण ‘सामान्य मानव की प्रतिष्ठा’ का सूचक है।
5. अन्य विशेषताएँ
बौद्धिकता, हास्य की अपेक्षा व्यंग्य की प्रधानता (शिवशंभु का चिट्ठा में बालमुकुंद गुप्त ने व्यंग्य लिखे, नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भरंडा रहस्य लिखा), आदर्शवादिता और नैतिकता द्विवेदीयुगीन काव्य की अन्य मुख्य विशेषताएँ थीं। भाषा की दृष्टि से द्विवेदी युग इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि इसने भविष्य की कविता के लिए एक वाणी दी जिसे हम ‘खड़ीबोली’ कहते हैं।
कतिपय आलोचकों ने द्विवेदीयुगीन काव्य पर नीरसता, इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, कविता में अपेक्षित गहराई एवं कलात्मक समृद्धि की न्यूनता इत्यादि के आरोप लागाए। यह स्थिति प्रारम्भिक वर्षों में अवश्य रही; परन्तु प्रियप्रवास (हरिऔध), साकेत (गुप्त), जयद्रथवध (गुप्त), भारत-भारती (गुप्त) इत्यादि रचनाओं को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
Search Queries:
द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं,द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता,द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं लिखिए,द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएँ, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं,dwivedi yugin kavya ki visheshtaen,dwivedi yugin kavya ki visheshta,
dwivedi yugin kavya ki pramukh visheshtaen,dwivedi yugin kavya ki visheshtaen bataiye,dwivedi yugin kavya dhara ki visheshta.
NET JRF HINDI PDF NOTES